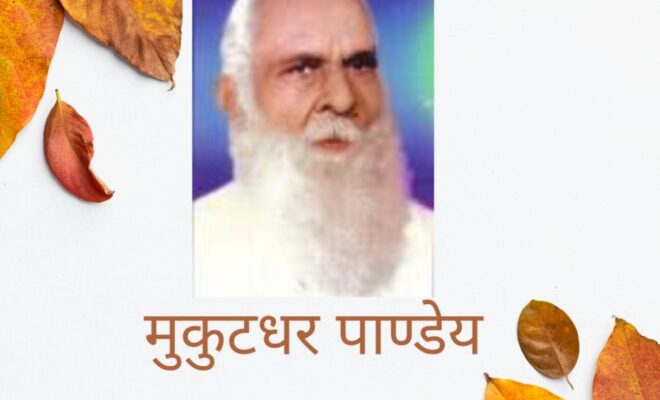चिन्ताओं से घिरा बाल साहित्य
बाल साहित्य के साथ कुछ ऐसी चिन्तायें जुड़ी हैं, जिनका वास्तविकता
से भले ही कोई लेना-देना न हो, किन्तु बच्चों के ज्ञान और मनोरंजन के परिक्षेत्र में यह अमरबेल की तरह
बेरोकटोक पैर पसारती जा रही है। प्रमुख चिन्ता बाल मनोविज्ञान को लेकर है। कहीं भी बाल साहित्य पर विमर्श
चल रहा हो तो चर्चा क्रम में कई ‘विद्वान’ यह तुक्का जड़ते मिल जायेंगे कि बाल साहित्य के सृजन में बाल
मनोविज्ञान का ध्यान रखा जाना चाहिये।
अच्छी बात है। कौन इससे असहमत हो सकता है ? जिस साहित्य में
बच्चा स्वयं को व्यक्त होता नहीं पायेगा, उसे वह भला क्यों पढ़ेगा ? मगर इस चिन्ता का खोखलापन तब प्रकट
हो जाता है, जब इसके प्रस्तावक ही उद्घोष करते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज या खाली प्लेट के
समान होता है। विचारणीय है कि अगर बच्चे का मस्तिष्क एकदम खाली है तो फिर बीच में बालमनोविज्ञान
कहाँ से टपक पड़ा ? ऐसी स्थिति में आप स्वतन्त्र हैं, उस कोरे कागज पर बच्चे के चरित्र, अभिवृत्ति और संस्कार
की मनचाही इबारत लिख डालिये। मगर क्या यह सम्भव हो सकता है।
असल में हम पश्चिम से आयातित विचारों के इतने गुलाम बन चुके
हैं कि हमारे पास जो अपना है, उसे हीन और हेय बनाने में अपना गौरव समझते हैं। अन्यथा क्या हमें
अभिमन्यु की कहानी नहीं पता है ? इसे कपोलकल्पित सिद्ध करने की बड़ी चर्चायें होती हैं। हम में से कितनों
का तर्क यह होता है कि यदि ऐसा पहले हुआ था तो अब क्यों नहीं होता ? इस कथा के अन्तर्निहित तत्व का
विधिवत् उद्घाटन कोई नहीं करना चाहता। महाभारत के रचनाकाल करीब छठीं सदी ईशा पूर्व में भारतीय
चिन्तन यह अन्वेषित कर चुका था कि बच्चा गर्भ से ही सीखना प्रारम्भ कर देता है। इसी तथ्य को
महाकाव्यकार व्यास जी अभिमन्यु की कथा का रूपक बनाकर भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया था।
आधुनिक मनोविज्ञान भी वंशानुगत से प्राप्त अभिक्षमताओं को स्वीकार
करता है। एकलव्य का धनुर्विद्या अर्जन का ही प्रसंग ले लें; यह द्रोणाचार्य की मूर्ति-प्रताप से सम्भव नहीं हुआ
था। एकलव्य की सफलता के पीछे उसकी जन्मजात और प्रत्येक बच्चे में पायी जाने वाली न्यूनाधिक
प्राणशक्ति का योगदान था। मनोविज्ञान का क, ख, ग जानने वाले को भी यह बताना आवश्यक नहीं कि बच्चा
जन्म से चौदह मूल प्रवृत्तियाँ लेकर पैदा होता है। प्रत्येक शिशु के मूल प्रवृत्यात्मक दबाव भी भिन्न होते हैं। यह
भिन्नता मूल प्रवृत्तियों के ज्ञानात्मक भावनात्मक एवं क्रियात्मक विभिन्नतायें बच्चे के पृथक् स्थायी भाव का
विकास करती हैं और यहीं उसके चरित्र निर्माण का प्रस्थान विन्दु होता है। इसीलिए सभी बच्चे एक सदृश्य या
विशेषताओं के नहीं होते, अपितु उनमें व्यक्तिगत अन्तर पाये जाते हैं।
यद्यपि यह सत्य है कि आधुनिक मनोविज्ञान जैसा व्यवस्थित और
क्रमबद्ध नहीं है। बालक की प्रकृति सम्बन्धी भारतीय चिन्तन, किन्तु महाकाव्यों, पुराणों और उपनिषदों में
बच्चों के स्वतन्त्र अस्तित्व और मौलिक विशिष्टताओं को सामने लाने वाली भारतीय मान्यताओं का परिचय
मिल सकता है। अब आधुनिक मनोविज्ञान भी बच्चे की लघु मानव सम्बन्धी मान्यता को त्याग चुका है। यह
भी स्मरणीय है कि बच्चा जन्म के साथ ही रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और ध्वनि से सीखना शुरू कर देता है। ऐसी
स्थिति में एकमात्र ‘लोरी’ को छोड़कर साहित्य के अन्य रूपों के पास पहुँचने के पूर्व वह काफी कुछ सीख चुका
होता है।
वस्तुतः रूसो का अप्रशिक्षित लघुमानववाद हो या जाँन लाक का
‘कोराकागजवाद’ यह दोनों सिद्धान्त विज्ञानसम्मत ही नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं
उठता। फिर भी इनके माध्यम से बचपन को संस्कारित करने का जो दुराग्रहचल रहा है, उसे रोकने-थामने को
कोई राजी नहीं है। क्योंकि प्रथमतः यह सिद्धान्त पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित है। इसलिए पश्चिम के
अंधानुकरण के नाम पर इनके समक्ष श्रद्धावनत होना हमारी मजबूरी है। दूसरे यह अभिभावक, शिक्षाशास्त्रियों
और राष्ट्र निर्माताओं को अपने खण्डित स्वप्न, इच्छा-आकांक्षा और सुन्दर भविष्य की कल्पना को साकार करने
का दार्शनिक आधार देता है।
बाल साहित्य की संरचना के सन्दर्भ में कई विद्वान पारस्परिक कथ्य और शिल्प वाली रचनाओं की निरन्तरता
पर चिन्ता जताते हैं। वे बाल साहित्य को शत-प्रतिशत यथार्थ से जुड़ा देखना चाहते हैं। निश्चय ही बच्चों के
साहित्य का परिवेश उनका जाना पहचाना होना चाहिये। निश्चय ही बच्चों के साहित्य का परिवेश उनका जाना
पहचाना होना चाहिये। इसका आधार विज्ञानसम्मत हो तो सोने में सुहागा। सूचना विस्फोट के इस कालखण्ड में
बच्चों का संज्ञानात्मक पक्ष खूब विकसित हुआ है। तदनुरूप रुचियाँ बदली हैं। कुतूहल और जिज्ञासाओं का
क्षितिज विस्तार हुआ है।
यह सत्य है कि इसे अपमार्जित नहीं किया जा सकता परन्तु इसे और गतिशील बनाने का उपक्रम क्या ठीक
माना जाना चाहिये ? आज का सामाजिक जीवन किस राह पर चल निकला है, यह बताने की बात नहीं है।
इसके बीच ही तो बच्चा पल रहा है। राग-द्वेष, बेईमानी, स्वार्थ, छल-कपट, हिंसा, छीना-झपटी, गलाकाट
प्रतिस्पद्र्धा जैसी निम्न वृत्तियों से बच्चों की मूलप्रवृत्तियों के संवेग क्रिया करके जिन संस्कारों का बीजारोपण
कर सकते हैं और उनसे जिन स्थाई भावों का निर्माण संभव है है, उसकी सम्भाव्यता को क्षीण करने की शक्ति
कहीं है तो वह पारम्परिक साहित्य में निहित है। क्योंकि यह कलपना के नये क्षितिज उपलब्ध कराता है, कुछ
समय के लिए वह वर्तमान जीवन के उजाड़ से मुक्त होकर सृष्टि के साथ जुड़कर एक नया सम्बोध ग्रहण
करता है। यह उसकी रागात्मक वृत्तियों, सौन्दर्यबोध और भावनाओं को विस्तार मिलने की सम्भावना अधिक है।
यह वह प्रक्रिया है जो उसे भावी जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में सन्तुलन रखने की
योग्यता प्रदान करती है। बदलते परिवेश के बीच समायोजन करने की योग्यता के विकास का यही प्रस्थान
विन्दु है। आधुनिकता से ग्रस्त साहित्य में यह शक्ति कम दिखती है। ऐसी स्थिति में पारम्परिक साहित्य को
आधुनिक परिवेश से जोड़ने की बात तो की जा सकती है, निकाल बाहर करने की नहीं। इस विषय में लम्बे
समय से कार्य हो रहा है।
बाल साहित्य के विकास के इतिहास के जानकारों को अच्छी तरह पता है कि हिन्दी में बच्चों की
पहली पत्रिका बाल दर्पण सन् 1882 में प्रकाशित हुई थी। तब से आज तक सैकड़ों बाल पत्रिकायें बाल साहित्य
को युग सापेक्ष, मूल्यपरक, सोद्देश्य, मौलिक और बाल रुचि के अनुकूल बनाने की दिशा में अपना सार्थक
योगदान देती आई हैं स्वतन्त्रता से पूर्व पं0 रामजी लाल शर्मा (विद्यार्थी), पं0 सुदर्शनाचार्य (शिशु), पं0 बदरीनाथ
भट्ट, लल्ली प्रसाद पाण्डेय, कामता प्रसाद ‘गुरु’, ठा0 श्रीनाथ सिंह (बालसखा), आचार्य रामलोचन शरण, रामवृक्ष
बेनीपुरी, आचार्य शिवपूजन सहाय (बालक), पं0 रामनरेश त्रिपाठी (वानर) द्वारा जिस प्रकार के रंजक
मनोविज्ञानपरक और मूल्यसंवर्धक बाल साहित्य को पहचान प्रदान की गई थी, स्वतन्त्रता के पश्चात् उसे
प्रतिष्ठित करने में आनन्द प्रकाश जैन, कन्हैयालाल नन्दन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हरिकृष्ण देवसरे (पराग),
जयप्रकाश भारती (नन्दन), दयाशंकर मिश्र दद्दा (राजा भैया), योगेन्द्रकुमार लल्ला (मेला), राधेश्याम प्रगल्भ (बाल
मेला) राष्ट्रबन्धु (बाल साहित्य समीक्षा) कृष्णकुमार आस्थाना (देवपुत्र) डा भैरूलाल गर्ग (बाल वाटिका) जैसे
अनुभवी और प्रखर सम्पादकों का प्रदेय उल्लेखनीय है। इसी क्रम में डा श्रीप्रसाद, विजयलक्ष्मी सिन्हा, निरंकार
देव सेवक, डा सुरेन्द्र विक्रम, डा शेषपाल सिंह ‘शेष’, उषा यादव, क्षमा शर्मा, अलका आर्य, प्रकाश मनु आदि
विद्वानों के आलोचनात्मक व मूल्यांकनपरक लेखों से बाल साहित्य विकास की नई त्वरा गति और प्रोत्साहन
प्राप्त करता आया है। यह करीब सवा सौ साल पुरानी बाल साहित्य की परम्परा है जो निरन्तर प्रवहमान है।
इसे रचनात्मक और मूल्यांकन के स्तर पर सम्पुष्ट करने के लिए नवागतांे का सिलसिला थमा नहीं है।
पारम्परिक बाल साहित्य विशेषकर को लेकर विचारकों में कई चिन्तायें हैं। उदाहरणार्थ लोककथायें सामंती
मूल्यों की पोषक है। परीकथाओं की संरचना अतिकाल्पनिकता के धरातल पर हुई है। मिथकीय और ऐतिहासिक
वांड़्मय की कहानियाँ साम्प्रदायिक मूल्यों का सम्प्रेषण करती हैं। इन चिन्ताओं पर भी एक संश्लेषणात्मक
दृष्टि डालना प्रासंगिक होगा। एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या समस्त लोककथायें राजा-रानी विषयक हैं
? पशु-पक्षी, किसान, मजदूरों, विद्वानों और चालाक व्यक्तियों से जुड़ी कथायें क्या नहीं है ? फिर सामन्ती
पृष्ठभूमि वाली कहानियों के अन्यायी-अनाचारी सामंतगण अंततः सामान्य जन के बीच से उभरे नायक के हाथों
पराजित होते हैं। इस प्रकार का अंत सामन्ती मूल्यों की स्थापना नहीं, बल्कि संघर्ष की चेतना की सकारात्मक
मनोवृत्ति विकसित करता है।
परीकथाओं की काल्पनिकता बच्चों की मौलिक प्रवृत्ति से मेल खाने वाली स्थिति है। बच्चा अपने आप में एक
कल्पनाशील प्राणी होता है। संसार में एक भी ऐसा मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा नहीं मिलेगा जिसका एक
सघन कल्पना लोक न हो। इसमें विचरण करते हुए बच्चे अपनी अनेकों इच्छाओं, आकांक्षाओं, अभावों और
जिज्ञासाओं का समाधान करके मानसिक संतोष प्राप्त करते हैं। कल्पनालोक बच्चों लिए प्रकृतिप्रदत्त ऐसा उपहार
है, जो उसको विद्यालय परिवार और समाज से जाने-अनजाने लगने वाले आघातों को झेलने की ताकत प्रदान
करता है। परीकथाओं का कल्पना तत्व अपनी सकारात्मक तार्किकता से बाल मन की कल्पना में स्वाभाविक
हस्तक्षेप करके उसे उचित दिशा देने का कार्य करते हैं। यह अवश्य ध्यातव्य है कि परीकथाओं के कल्पना तत्व
अर्थपूर्ण और प्रेरणादायी हैं।
पौराणिक पात्रों, महाकावयों के प्रसंग, उपनिषद के रूपक, जातेक और जैन आगम कथायें, लोक नायक, इतिहास
पुरुष, संत परम्परा पर आधारित रचनायें हमारे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विरासत की संवाहक होती
हैं। इनके माध्यम से बच्चे अतीत के श्रेष्ठत्व से परिचित होते हैं। इनमें किसी की आलोचना, किसी को हीन
सिद्ध करने का प्रयास अथवा अपने विचारों को बलात थोपने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। यह अपनी गहन
अर्थधर्मी सांकेतिकता के प्रभाव से उच्च जीवन मूल्यों का प्रक्षेपण करके बाल पाठकों के व्यवहार, संस्कार, चिंतन
और वाणी को सृजनात्मक दिशा प्रदान करती हैं इन कथानकों में भावों का चमत्कार उच्च स्तर का होता है।
इन कहानियों का जो प्रदेय होता है अपने समेकित प्रभाव के अन्तर्गत वह किसी भी धार्मिक समुदाय के लिए
घातक नहीं हो सकता।
प्राचीन साहित्य की प्रासंगिकता न खत्म हुई है न ही होगी। इसे बच्चों के साहित्य से निकालकर करने की बात
तो सोची ही नहीं जानी चाहिये। अधिक से अधिक पुरातन स्रोतों से सामग्री लेकर तैयार किये जाने वाले बाल
साहित्य केा आधुनिक बच्चों की परिवर्तित रुचि और जिज्ञासाओं के अनुकूल परिवर्तित और संशोधित करने का
चिन्तन युग सापेक्ष है। लोक साहित्य हो या मिथकीय साहित्य, यह तभी बालोपयोगी हो सकता है जब इसे
आधुनिक जीवन स्थितियों और भावबोध से जोड़ा जाए, इससे किसी को इंकार नहीं हो सकता।
काल के तीनों आयामों – भूत, वर्तमान और भविष्य- की उपस्थिति ही साहित्य को साहित्य बनाती है। इसलिए
बच्चों के साहित्य में अतीत के श्रेष्ठत्व का गौरव, वर्तमान की चुनौतियाँ और भविष्य के स्वप्न हों, तभी वह
प्रासंगिक और लोकप्रिय हो सकता है। इसके लिए चिन्ताओं को दरकिनार करके विशुद्ध चिन्तन करना होगा-
इसी में इसकी संभाव्यता निहित है।