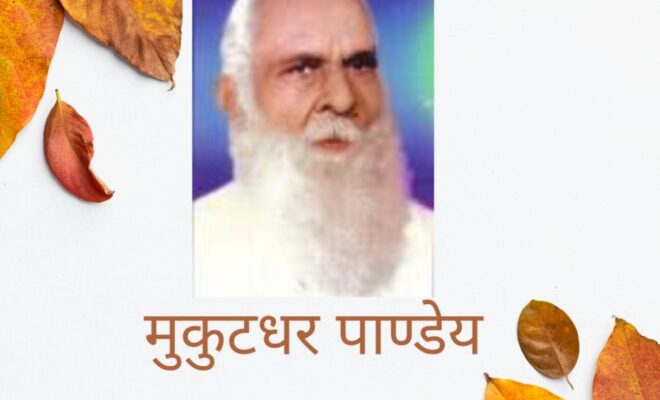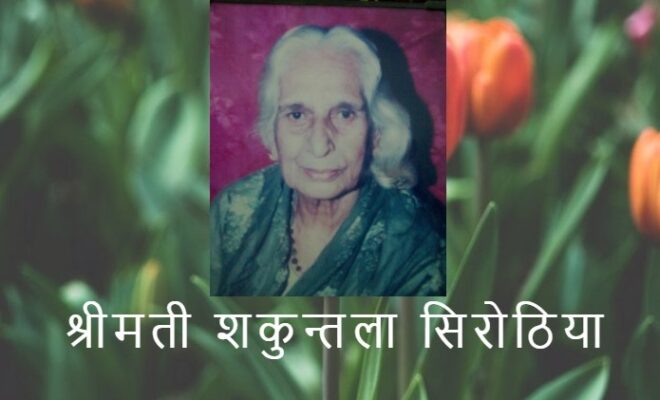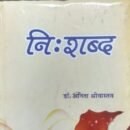टीवी के आगे बच्चा

आज टी.वी. का सबसे बड़ा दर्शक वर्ग बच्चे हैं। यह खूब मस्त होकर टीवी के
आगे सुध-बुध खोये रहते हैं। अभिभावक आश्वस्त हैं कि बच्चा टीवी देख रहा है; कुछ नया देख, समझ और
सीख रहा है। शरारत नहीं करेगा। मगर दूरदर्शन से अत्यधिक लगाव और अन्तरंगता कई एक मनोदैहिक
समस्यायें भी पैदा कर रही हैं।
अधिक समय तक टीवी देखने से बच्चों में सिरदर्द, गर्दन व पीठ में अकड़न की
शिकायत मिलती है। यह दिक्कत तब और बढ़ जाती है, जब वे टेलीविजन देखते समय उचित ढंग और स्थान
पर बैठने की सावधानी नहीं अपनाते। कम उम्र के बच्चे अगर स्कूल जाने से पहले अधिक टीवी देखते हैं तो
उन्हें आँखें स्थिर रखने की आदत पड़ जाती है। जबकि पढ़ने के लिए उन्हें शब्द-दर- शब्द आँखों को गतिशील
बनाने की आवश्यकता होती है। आँखों की स्थिरता उनके पढ़ने की गति में अवरोध का कार्य करती है। छोटे
बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं तो हाथों का कई उपयोग करते हैं। इससे उनका पेशीय नियन्त्रण सुदृढ़ होता है।
मगर टीवी देखते समय उनके हाथ घंटों निष्क्रिय रहते हैं, यह उनके सीखने की क्षमता, विशेषकर सुलेखन और
चित्रकारी पर बुरा असर डालता है।
दूरदर्शन के कार्यक्रमों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश कार्यक्रम भौड़ी
कामेडी, षड्यन्त्र, हिंसा, अपराध और सेक्स पर आधारित होते हैं। उच्च वर्ग और राजघरानों की संस्कृति को गाँव-
घर की संस्कृति बनाकर पेश किया जा रहा है। बालमन इसे ही आत्मसात कर रहा है। नतीजतन समाज में
नंगापन, विदू्रपता, हिंसा और अश्लीलता बढ़ रही है। संवेदना का स्तर कमजोर हो रहा है। लाज-हया और लिहाज
के बन्धन ढीले पड़ चुके हैं। संस्कारों पर आधारित जीवन-मूल्यों का लोप होने लगा है। कच्ची उम्र में ही बच्चों
में शराब, सिगरेट और देह का आकर्षण बढ़ रहा है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों में जीवन के नकारात्मक पक्षों का
प्रयोग जिस गति से बढ़ रहा है, उसी पैमाने में बच्चों के जीवन में विद्रूपतायें जन्म ले रही हैं। इसका कारण यह
है कि बच्चे बिना तर्क-वितर्क किये टीवी के कार्यक्रमों के संदेशों और दृश्यों को सत्य मान लेते हैं और जीवन में
उसकी नकल उतारते हैं।
कहा गया है, बच्चे का मस्तिष्क संसार की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ सदैव कुछ न कुछ
नया होता रहता है। निरन्तर हिंसात्मक दृश्यों को देखते हुए बच्चों में हिंसा का पनपना स्वभाविक है। हिंसा से
भरा हुआ मस्तिष्क प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के लिए सदैव तैयार रहता है। जबकि सूझबूझ, विवेक और बौद्धिक
कार्यों के सन्दर्भ में यह एकदम ऊसर जैसा होता है। इधर बच्चों में हिंसक वृत्तियों का जैसा ग्राफ बढ़ा है, आए
दिन बच्चे अपने अध्यापकों, साथियों और परिजनों पर गोलियाँ तक चला रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति की
परम्पराओं में एक नया मोड़ है।
टीवी संस्कृति के कारण बच्चों में मोटापा जैसी विकृतियाँ बढ़ रही हैं। दरअसल बच्चे टेलीविजन देखने के
चक्कर में खेलकूद और व्यायाम भूलते जा रहे हैं। स्कूल से घर लौटने पर वे टीवी के सामने बैठ जाते हैं। यही
नहीं, वे टेलीविजन देखते समय तली-भुनी चीजें भी खाते रहते हैं। इससे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती जाती है।
मोटे हो रहे यही बच्चे भविष्य में मधुमेह, उच्च रक्त चाप और हृदयाघात जैसी बीमारियों के घेरे में आ सकते
हैं।
खेलकूद बच्चों के शारीरिक विकास को संतुलित रखता है। यह मानसिक, शैक्षणित और
भावनात्मक विकास के लिए भी आवश्यक है। यहाँ तक कि खेलकूद से बच्चों में सामाजिकता और व्यवहारगत
कुशलता भी विकसित होती है। मौजूदा वक्त में टीवी के चलते बच्चों के बीच खेलकूद का लोप एक बड़ी चुनौती
है। क्योंकि खेलों के अभाव के बीच सयानी होती पीढ़ी में आने वाले समय में कलात्मक और सृजनात्मक
गतिविधियों में ह्रास की सम्भावना है।
बालरोग विशेषज्ञों और मनोविज्ञानवेत्ताओं का मत है कि बच्चों को दिन भर में दो-ढाई
घंटे से अधिक समय टीवी नहीं देखना चाहिये। जबकि बच्चे देर रात तक टीवी देखते रहते हैं। खासकर मैच
सम्बन्धी प्रसारण वाले दिनों में यह सीमा बहुत बढ़ जाती है। इससे बच्चों के पढ़ाई और होमवर्क के स्तर में
कमी आ रही है। इसमें समय के अभाव की ही बात नहीं है, बल्कि दूरदर्शन की अधिकता से मस्तिष्क की
सृजनात्मक व तार्किक क्षमता एवं एकाग्रता में आने वाली कमी भी जिम्मेदार है।
तमाम कमियों के बाद भी यह नहीं भूलना चाहिये कि टीवी एक सशक्त माध्यम है।
अगर इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल हो तो यह शिक्षा, जागरूकता और स्वस्थ मनोरंजन का कारगर साधन हो
सकता है। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, जागरूक नागरिकों, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को
सरकार पर दबाव बनाना चाहिये कि देश में दूरदर्शन सम्बन्धी एक ठोस नीति तैयार हो, जिसके तहत मनोरंजक,
शिक्षाप्रद, सूचनात्मक, भारतीय जीवन मूल्यों और भारतीयता के पोषक कार्यक्रम तैयार किये जायें।
जब तक ऐसा बदलाव नहीं आता, परिवार की आपसी सहमति से केवल अच्छे
कार्यक्रम देखने की समझ पैदा करनी होगी। आपसी विचार-विमर्श में बच्चों की बराबरी की भागीदारी होनी
चाहिये, ताकि वे सहजता से यह फैसला स्वीकारें और अपने सहपाठियों-मित्रों से इस सन्दर्भ में चर्चा करके इसके
प्रसार में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें।