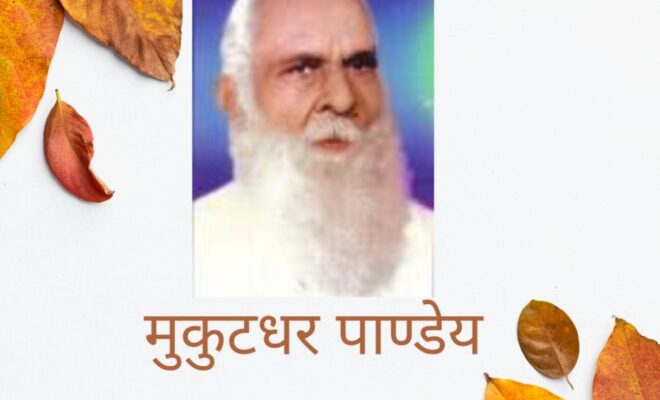इतिहास के पन्नों से लुप्त होते साहित्यकार : बन्दे अली फातमी
कलमकी तलवार पकड़े इन साहित्यिक सिपाहियों ने समय-समय पर गांधीजी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी निभाई है। विदेशी वस्त्रों का त्याग किया तो सरकारी नौकरियां भी छोड़ीं। जेल गए और शासन के कठोर दंड भी सहे। आजादी की इस लड़ाई में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जनपद से भी एक ऐसा नाम है, जिसका यह जन्म शताब्दी वर्ष है और वह नाम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गीत-गजलकार बन्दे अली फातमी का। बन्दे अली फातमी का जन्म 12 नवम्बर 1912 में रायगढ़ के एक रईस परिवार में हुआ था। गौर वर्ण, लगभग छ: फीट से अधिक लंबाई वाले कवि व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फातमीजी हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू, अरबी, फारसी और बंगला भाषा साहित्य पर भी समान अधिकार रखते थे। वे हिन्दी के छंद व उर्दू कविता की तमाम बारीकियाें से वाकिफ थे।
फातमीजी के पिता मुल्ला फखरुद्दीन अली की गिनती रायगढ़ के सेठों में होती थी। किंतु देश भक्ति का जुनून जिस पर सवार हो, वह भला संपत्ति कहां संभाल सकता है, वही फातमीजी के साथ हुआ। पिता के निधन के पश्चात वे सियासत की लड़ाई के साथ विरासत में मिली दौलत व व्यापार को बढ़ा नहीं सके। समय का पांसा पलटा और फातमीजी की दुकानें बिक गईं। व्यापार ठप्प हो गए और रह गया शहर में रहने को मात्र एक पक्का मकान।
अब तक वे आजादी की यात्रा में शामिल हो चुके थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने व स्वदेशी धारण करने की अलख जगाने हेतु घर से बाहर निकल पड़े थे। 1930 में जब गांधीजी बिलासपुर आये थे, तब वहां के प्रतिनिधि मंडल में बंदे अली फातमी भी थे। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए कवि हृदय फातमीजी के गीत-गजल भी समाज में अपना किरदार निभा रहे थे।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेजी हुकूमत के साथ-साथ राजशाही शासन का भी कोपभाजन बनना पड़ा था, जिससे फातमीजी अछूते नहीं रहे। 1930 में बिलासपुर व 1933 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह में रायगढ़ से शामिल होने वाले फातमी को भी तत्कालीन सत्ता के जुल्म को सहना पड़ा। लेकिन इन तमाम यातनाओं से जूझते हुए भी कवि फातमी की आवाज हमेशा बुलन्द थी जो उनकी कविताओं में स्पष्ट झलकती है। तभी तो वे कहते हैं-
दौलते हुकूमत का जो भी करता है इस्तेमाल गलत
होता है उसका हाल गलत, होता है उसका चाल गलत
ये फातमी जो भी नशे में हो कह दो कि होश में आ जाये
अंजाम नहीं होता अच्छा, होता है अगर इस्तेमाल गलत।
रायगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लंबी फेहरिस्त में जब सिध्देश्वर गुरु, राम कुमार अग्रवाल, किशोरी मोहन त्रिपाठी, लाला फूलचंद, तोड़ाराम जोगी, अमरनाथ तिवारी, बैजनाथ मोदी आदि का नाम लिया जाता है तो यह सूची बंदे अली फातमी के बगैर अधूरी रह जाती है। आजादी की लड़ाई में फातमीजी प्रत्येक मोर्चे पर आगे रहे।
कवि हृदय फातमीजी की पहली गज् ाल अज्ञेयजी के सम्पादन में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी-
बिना देखे हृदय को हार डाला
अरे सर्वस्व पी पर वार डाला
न जाने किंतु मेरा पी कहां है
पपीहे, पी कहां ने मार डाला।
इसके पश्चात बहुत सी गजलें तत्कालीन पत्रिकाओं में विशेष कर हंस, चांद, माधुरी, कर्मवीर, सुकवि, सरस्वती आदि में प्रकाशित होती रही। लेकिन उनका व्यक्तिगत कोई संकलन नहीं निकल पाया। उनका मानना था कला की दृष्टि से उर्दू में गीत लिखे जा सकते हैं तो हिन्दी में गज् ाल भी कही जा सकती है।
गीत गज् ाल के रचयिता फातमीजी कभी किसी साहित्यिकवाद या गुटबंदी में नहीं पड़े। उनके काव्य की केन्द्रीय सोच मानवीय प्रेम है। वे संपूर्ण जगत को प्यार से बांधना चाहते थे। तभी तो एक सच्चे नेकदिल इन्सान फातमीजी कहते हैं-
सुन लो अय दुनिया वालाें क्या है मेरी चाहों में
जगती को बांध रहा हूं प्यार भरी बाहों में।
रायगढ़ का सांस्कृतिक वैभव (डॉ. बलदेव साव) पढ़ते समय मैंने बन्दे अली फातमी के विषय में भी पढ़ा। फिर मुझे लगा कि फातमीजी के विषय में कुछ और जानकारी मिलती तो अच्छा होता और कहते हैं न कि जहां चाह वहां राह। सच है कि मुझे वह राह दिखाई पड़ी और मैं पहुंच गया राहगीरजी के निवास पर अर्थात् अमीरचंद अग्रवाल राहगीर।
मैं जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार जनकवि आनन्दी सहाय शुक्लजी से मिला। उन्होंने बताया बन्दे अली फातमी एक सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देश की आजादी के लिए वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे। फातमीजी के पिता फखरुद्दीन रायगढ़ के सेठों में थे, जिनके पास कई मकान व दुकानें थीं। उनको लेकर एक कहावत थी कि-
तांबाजस्ताटीन
गली-गली में फखरुद्दीन।
अर्थात् प्रत्येक क्षेत्र में सेठ फखरुद्दीन का दबदबा था। लेकिन फातमीजी उसे संभाल नहीं सके क्योंकि उन्हें देश की आजादी के प्रति भूत सवार था। माननीय शुक्लजी ने आगे कहा फातमीजी ने वेद, पुराण व उपनिषद का भी अध्ययन किया था। उन्हें संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदीजी का साप्ताहिक कर्मवीर, जो देश में आजादी की मशाल समझा जाता था। फातमीजी इस पत्र में अंग्रेजों व रियासत के विरुध्द लगातार लिखा करते थे, जिसका प्रभाव जनमानस पर साफ दिखता था। यहीं नहीं, उनके लेखों से जनपद का राजतंत्र इतना नाराज हुआ था कि एक बार जब फातमीजी नगर के एक व्यवसायी के यहां बैठे थे तो उस समय राजतंत्र के कुछ पहलवानों ने फातमीजी पर प्राणघातक हमला कर दिया और अंत में मरा समझ कर ही छोड़ कर गए। उस हमले में फातमीजी बच तो गए लेकिन जीवन भर उनका दाहिना हाथ कमजोर रहा। इस हमले के बाद भी उनके जज् बे में कोई कमी नहीं आई। जीवन भर उन्होंने खादी पहनी और देश के प्रति समर्पित रहे।
फातमीजी के साहित्यिक योगदान की चर्चा करते हुए आनन्दी सहाय शुक्लजी कहते हैं कि फातमीजी ने हरिद्वार में हुए साहित्य सम्मेलन में भाग लिया था। ‘राष्ट्र केशरी’ व ‘नई बात’ साप्ताहिक का सम्पादन करते हुए भी उनकी भूमिका हमेशा शोषितों व दलितों के लिए प्रशासन से दो-दो हाथ करने की रही। उनका जीवन बहुत कष्टों से भरा था, लेकिन वे स्वाभिमान के प्रतीक थे। तभी तो कहते थे-
मैं गाता हूं सांसों का स्वर
मोहताज चांद सूरज का क्यों
जब खुद ही प्रकाश का घर हूं मैं।
उनकी सबसे लोकप्रिय कविता मुरली और शंख के बारे में शुक्लजी ने कहा कि जब-जब समाज को माधुर्य कोमलता व स्नेह की आवश्यकता पड़ी तब मुरली सामने आयी और जब सिध्दांत के लिए जूझने की जरूरत होती है तो शंख निनाद होता है।
वरिष्ठ साहित्यकार व आलोचक डॉ. प्रभात त्रिपाठी ने बताया कि बन्दे अली फातमी बहुत अच्छे कवि थे। वे बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने जीवन में तमाम उतार-चढ़ाव देखे किंतु कभी किसी से निजी जीवन का इश्तहार नहीं किया। उनके गीतों में गेयता थी, रायगढ़ के एक बड़े सेठ व साहित्य प्रेमी श्री नत्थूलाल गुप्त तो फातमीजी के गीतों को सस्वर गाते थे। डॉ. त्रिपाठीजी ने अपने पिता किशोरी मोहन त्रिपाठी (जो रायगढ़ के सांसद व साहित्यकार थे) का जिक्र करते हुए कहा कि पिताजी को दोहों के प्रति फातमीजी से ही प्रेरणा मिली।
एक आलोचक की दृष्टि से त्रिपाठीजी ने कहा कि फातमी की कविता में छायावादी प्रभाव स्पष्ट नहीं था, जैसा कि उस समय के लोगों में था। उन पर माखनलाल चतुर्वेदीजी का प्रभाव अवश्य था। फातमीजी को राष्ट्रभक्ति व ईश्वरभक्ति एक ही लगती थी। वे उर्दू की तहजीब से वाकिफ थे, लेकिन उनकी भाषा के संस्कार पूरी तरह से हिन्दी और संस्कृत के थे। वे निराला की परम्परा में लिखते थे। उनकी संस्कृति लूट की होती है। तबाही की होती है। अंग्रेज जो नफरत का बीज बोकर गए थे। उसकी फसल एक बार रायगढ़ शहर में भी 1964 काटी गई। घोर तबाही लूटपाट आगजनी। बन्दे अली फातमी का घर भी लूटा गया। उनकी साहित्य की समृध्द लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। महल में रहने वाले फातमी सड़क पर आ गए। अंतिम दिनाें में उन्हें बहुत गरीबी भी देखनी पड़ी।
कठिन संघर्षाें में भी फातमीजी ने साहित्य का दामन नहीं छोड़ा था। 1940 में हरिद्वार में आयोजित भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में बन्दे अली फातमी ने भाग लिया। वहां उनकी प्रंशसा में सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था ‘बन्दे अली फातमी स्नेह स्निग्ध वाणी के दूत, युग लेखन में प्रखर व सजग है।’
कृष्ण और राधा को जिसने चाहा वह भला कृष्ण के गीता उपदेश को कैसे भुला सकता है- कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परिणाम की चिंता किये बगैर फातमीजी ने वह सारे कार्य किये जो सर्वमान्य थे। वे मानते थे व्यक्ति समाज और राष्ट्रहित के लिए संघर्ष ही सार्थक जीवन का उद्देश्य है। किंतु जीवन भर प्रेम और जागरण के गीत गाने वाले फातमी अपने अंतिम दिनों में निराश थे। तन-मन-धन अर्थात् सब कुछ राष्ट्र के लिए न्योछावर करने वाले बन्दे अली फातमी सदैव उपेक्षित रहे।
देश के वास्ते मैं भी कभी अनुरक्त रहा
अपने उन प्यारे विचारों में आसक्त रहा।
मुझको न समझा किसी ने, न चाहा किसी ने
व्यक्त मैं इतना हुआ फिर तो अव्यक्त रहा।
सत्तर वर्ष के संघर्षमय जीवन में उन्होंने इतने थपेड़े सहे। इतनी यातनाएं झेलीं कि लगा अंत में निश्छल, निष्कपट व्यक्तित्व के बन्दे अली फातमी छलकपट के चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा घिर गऐ हैं:-
ये कहना कठिन है कि कहां तक गया हूं
मगर इतना सच है कि बहुत थक गया हूं
न रोपा गया और न सींच गया जो
उसी वृक्ष का आम हूं मैं पक गया हूं।
एक रईस खानदान के महल में जन्मे बन्दे अली फातमी एक गरीब की कुटिया से 22 नवम्बर 1981 को इस दुनिया से विदा हो गए। फातमीजी के मात्र दो पुत्रियां हैं जो संभवत: इन्दौर में रहती हैं। प्राप्त लेखों व कुछ जानकारों से ज्ञात हुआ कि उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए शव यात्रा में बमुश्किल आठ-दस लोग थे। लेकिन जिसने फातमीजी के जीवन संघर्ष की गाथा को पढ़ा है जो भी रायगढ़ से स्वतंत्रता की लड़ाई को जानता है, उनके त्याग व बलिदान के महत्व को जानना है। वह भला कैसे भूल सकता है, बन्दे अली फातमी को। गतवर्ष उनका जन्मशताब्दी वर्ष था। ऐसे अवसर पर उन्हें सादर नमन करते हुए मैं अपनी श्रध्दांजलि अर्पित करता हूं।